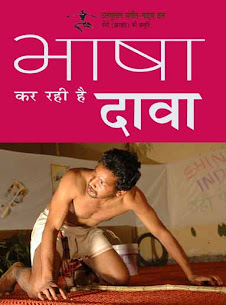रंगकर्मी ब॰ व॰ कारंत अब हमारे बीच नहीं हैं। लेकिन न सिर्फ़ हिंदी और कन्नड़ बल्कि भारतीय रंगमंच में उनका जो अवदान है वह न सिर्फ़ अविस्मरणीय है, मील का पत्थर भी है। संगीत भी वह साधते थे और कहते थे कि नाटक पॉपुलर होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है गर्मी पैदा करना। वह जब आखि़री बार लखनऊ आए थे तो एक नाट्य प्रतियोगिता में शिरकत के लिए। उनकी सादगी और सक्रियता देखते बनती थी। तभी राष्ट्रीय सहारा के लिए ब॰ व॰ कारंत से दयानंद पांडेय ने एक ख़ास बातचीत की थी। पेश है वह बातचीत:
प्रसिद्ध निर्देशक और रंगकर्मी ब॰ व॰ कारंत का कहना है कि मैं हीरो वाले नाटकों को बहुत कम पसंद करता हूं। मैं करता नहीं। अब कि जैसे भारतेंदु का अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक मैंने किया। इसमें कोई हीरो नहीं। इसमें सरकारी तंत्र पर जो व्यंग्य किया गया है, इस नाते यह हमेशा प्रासंगिक रहता है। ‘कल्लू बनिए को पकड़ लाओ जी’ जैसे संवादों के मार्फत अंधेर नगरी सिर्फ़ हास्य नाटक नहीं, व्यंग्य हो जाता है। और आज के हालात पर, त्रासदी पर इससे सटीक व्यंग्य मुझे नहीं दिखता।
कारंत कहते हैं कि इसी तरह कालिदास की शकुतला मेरे लिए आज भी प्रासंगिक है। क्यों कि दुष्यंत आज भी शकुंतला को धोखा देता मिलता है। डेढ़ सौ साल पहले का यह नाटक है। पर शकुंतला पुरूष के लिए आज भी जंगली चीज़ है। शुरू में जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मैंने इन नाटकों को उठाया तो इन नाटकों के बारे में बहुत सारी शंकाएं उठाई गईं। अब पाता हूं कि मेरी बहुत सारी पुरानी धारणाएं निरंतर टूटती जाती हैं। खैर इस पर बात ज़रा आगे। पहले हम लोग कहते थे कि नाटक करना पैदाइशी है। पर अब मानते हैं कि सीखना चाहिए। और फिर भी इस सबके बावजूद भरतमुनि से आगे हम नहीं बढ़ पाए हैं। खुशी है इस बात की। तो माडर्न नाटक क्या है? मेरे लिए अंतर नहीं पड़ता कि आज का नाटक तुगलक है कि कल का शकुंतला ! बस प्रासंगिकता रहनी चाहिए। तो नाटक में ट्रेनिंग ज़रूरी है कई बार तात्कालिक चीज़ों पर भी नाटक ठीक लगते हैं। जैसे मंडल आंदोलन चला तो उस पर भी नाटक हुए। गिरीश कर्नाड ने भी नाटक लिखा कन्नड़ में तलदंडा। फिर घासी राम कोतवाल, हयवदन बिलकुल भिन्न नाटक हैं। दरअसल, रंगमंच में समकालीनता की तलाश हो रही है। यह आज का ट्रेंड है। पर दिक्क़तें भी कई हैं। रंगमंच से संबंधित पत्रिकाएं पहले चलती थीं। और म्यूज़िकल कंसेप्ट की भी। नटरंग, नाट्य शोध आज भी है।
कारंत कहते हैं कि मैं माडर्न थिएटर नहीं मानता। समकालीनता को मानता हूं। जैसे महेश दत्तानी लिखते अंगरेज़ी में हैं पर समस्या हिंदुस्तानी लेते हैं। जाति-पांति का सवाल है। ये सारे सवाल अब नाटक में देखे जा सकते हैं। हां, तकनीक वेस्टर्न ले सकते हैं, कैसेट जैसी तकनीक लेना भी ग़लत नहीं है। किसी चीज़ को वेस्टर्न कह कर नहीं फेंक सकते। वस्तुतः रंगमंच का स्वरूप वेस्टर्न से काफी प्रभावित है। ब्रेख्त की बात करते हैं तो संसार के रंगमंच की भी बात करते हैं। रंगमंच में कमियां भी बहुत हैं हमारे। क्यों कि हिंदुस्तान में बहुत सी भाषाएं हैं। तो भाषागत विविधता होते हुए भी प्रशिक्षण के लिए एक ही स्कूल है नेशनल स्कूल ऑफ़ ड्रामा। यह ठीक नहीं है। हर क्षेत्र में, हर भाषा में नाटक की ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी ही चाहिए। पर दिक्क़त यह है कि आंध्र का कोई लड़का एन.एस.डी. में नाटक सीखने आता है तो अपनी भाषा से कट जाता है। जबरदस्ती हिंदी सीखनी पड़ती है। तो उसका सारा ध्यान नाटक से हट कर हिंदी पर आ जाता है। होना यह चाहिए कि देश के हर विश्वविद्यालय में नाटक पढ़ाने की व्यवस्था वहां की भाषा में ही होनी चाहिए। देश में सैकड़ों विश्वविद्यालय हैं पर अभी सिर्फ़ चालीस विश्वविद्यालयों में ही नाटक पढ़ाया जाता है। थिएटर में विश्वविद्यालयों का योगदान बहुत कम है। हालांकि थिएटर के लिए दो विश्वविद्यालय इन दिनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक त्रिचूर में और एक चंडीगढ़ में। एन.एस.डी. ने भी ब्रांचेज़ खोलने की कोशिश की। बेंगलूर में खोला। पर सरकार नाटक को महत्व नहीं देती। स्थिति यह है कि हमारे केंद्रीय बजट में संस्कृति पर सरकार सिर्फ़ 0.03 प्रतिशत ही खर्च करती है। तब जब कि दूसरे देशों में ठीक इसका उलटा है। लंदन में भाषा एक है। पर थिएटर सिखाने के लिए 16 संस्थाएं हैं।
कोई भाषा, कोई एक्टिंग, कोई संगीत ऐसे ही और कई चीज़ें वहां सिखाई जाती हैं। पर आप के लखनऊ में? भारतेंदु नाट्य अकादमी होते हुए भी हिंदी पर कितना काम हो रहा है। मैं नहीं समझता। बात एन.एस.डी के पुराने हो जाने की चली तो कारंत बोले, हम नहीं कह सकते कि एन.एस.डी. बुढ़ऊ हो गई संस्था है। नए-नए लोग आ रहे हैं। आज कल वर्कशाप ओरिएंटेड नाटक भी बहुत हो रहे हैं। अब वेस्टर्न में भी ऐसी ही रेपेट्री चलने लगी हैं। यह एक नया ट्रेंड है। एन.एस.डी. दिल्ली, भोपाल, रंगमंडल और बेंगलूर रंगमंडल अच्छा काम कर रहे हैं। आज भले गली-गली में नाटक न खेला जा रहा हो। पर चर्चा हो रही है।
थिएटर और मीडिया से कम्पेयर की जब बात चली तो कारंत का कहना था कि टी.वी. से ख़तरा है। थिएटर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। कोई भी समझदार आदमी थिएटर पर ध्यान नहीं दे रहा है। सेमिनार हो रहा है पर गर्मागर्मी नहीं। ठंडा हो गया है माहौल। टी.वी. का जाल इतना घना है कि असर पड़ गया है। इसी लिए नाटक कम हो गए। बड़े शहरों में नाटक नहीं हो रहा है। पर गांवों में हो रहा है। रंगमंच संबंधी लाइब्रेरी नहीं के बराबर हैं। एक एन.एस.डी. के पास है, दूसरा मेरे पास है। मेरे पास पांच हज़ार किताबें हैं थिएटर से संबंधित। तो यह मेरा व्यक्तिगत पागलपन है। पर कितने लोग नाटक पढ़ते हैं? मैं पटना गया था। तो कहा कि आप लाइब्रेरी खोलें तो पचास किताबें मैं दूंगा। पर किसी ने खोला नहीं। मैं सोचता हूं कि हर संस्था के पास अपनी होम मैगज़ीन होनी चाहिए। नाटकों पर चर्चा होनी चाहिए। पर ऐसा कुछ नहीं है। यह पूछने पर कि इस दिक्क़त को कौन दूर करेगा? तो कारंत बोले, शायद समाज ही। वह कहने लगे इतना सब होने के बाद भी रूस में आज भी नाटक ज़रूर पढ़ाया जाता है। संगोठियां ज़रूर होनी चाहिए। भले ही झगड़ा क्यों न हो। पर आज तक लोग जैसे गूंगे हो गए हैं। अब जरा ठंड बढ़ गई है बहस में।
बात फिर नाटकों की ओर वापस आई है। कारंत कहते हैं कि जब जयशंकर प्रसाद कहते थे कि रंगमंच के लिए नाटक नहीं, नाटक के लिए रंगमंच है। तो लोग यह बात मानते नहीं थे। लेकिन प्रसाद के स्कंदगुप्त के दर्जनों शो मैंने किए। दरअसल दुनिया में कहीं भी साहित्यिक और मंचीय नाटक का विभेद नहीं है। पर हिंदी में चला। खूब चला। यह ठीक नहीं है। नाटक, नाटक है।
वह कहते हैं कि मैं थिएटर के लिए हमेशा आशावादी रहूंगा। मैं भले ही रंगमंच से निवृत हो जाऊं, पर रंगमंच निवृत नहीं होगा। बात निर्देशक के निरंकुश होने की चली तो कारंत बोले मैं निर्देशक को दोषी नहीं पाता। यह कहने पर कि आप को नहीं लगता कि निर्देशक की मनमानी और उसके बूटों तले लेखक कितना कुचला गया, ख़ास कर हिंदी लेखक तो नतीजतन अच्छे नाटकों की निरंतर कमी होती गई। और अब अकाल पड़ गया है? कारंत बोले आप के प्रश्नों के पीछे बहुत पूर्वाग्रह है, इनका जवाब नहीं दे सकता। पर यह ज़रूर है कि निर्देशक को मैं दोषी नहीं पाता। अब किसी एक ख़ास समूह के लिए आप बात कह रहे हों तो बात और है। यह ज़रूर है कि आज रंगमंच में थोड़ी सी मंदी आ गई है। तो भी किसी न किसी रूप में नाटक करने की जो चेतना है। वह जागृत है। अभी आप पांडवानी और तीजनबाई की बात कर रहे थे तो क्या पांडवानी नाटक से बाहर है?
अल्काज़ी और शंभू मित्रा के बाद आप की पीढ़ी ने थिएटर की वह परंपरा नहीं खड़ी की? पूछने पर कारंत ने प्रति प्रश्न किया, आप ने यह नहीं पूछा कि हिंदी प्रदेशों से जो लोग एन.एस.डी. से ट्रेनिंग ले कर निकले वह लोग कहां गए? और फिर ड्रामा स्कूल अल्काज़ी से बहुत आगे जा चुका है। अल्काज़ी ने 16-17 वर्ष काम किया। पर अब वापस भी आ जाएं तो वह कुछ नहीं कर सकते। तो आप का यह सवाल मुझे ठीक नहीं लगता। और जो आप बार-बार अल्काज़ी-अल्काज़ी की रट लगाए हुए हैं। तो इधर एन.एस.डी. के लिए उन्होंने तीन नाटक किए। पर कन्नड़ नाटक अल्काज़ी अच्छा नहीं कर पाए, अल्काज़ी पकड़ नहीं पाए। मोहन राकेश के नाटक ‘आषाढ़ का एक दिन’ का एक संवाद है कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। तो समय अल्काज़ी के हाथ से निकल गया है। बात एन.एस.डी. में कारंत के कार्यकाल में आत्महत्याओं की चली, तो वह बोले, इससे रंगमंच का क्या? यह कहने पर कि यह सवाल आज भी वहां गूंजता है। कारंत का कहना था, वहां भी आदमी रहते हैं, मठ थोड़े ही है। आज तक किसी ने नहीं कहा कि एन.एस.डी. की ज़रूरत नहीं है।
आप को एक समय में थिएटर में लोक संगीत के प्रयोग के नाते हम लोग जानते थे। पर अब थिएटर से लोक संगीत का प्रयोग लगभग बिसरता जा रहा है। आप को क्या लगता है? कारंत बोले ख़त्म होना स्वाभाविक है। क्यों कि पहले वेस्टर्न से प्रभावित था हमारा थिएटर, तो वह बदलाव ज़रूरी था। अपनी पहचान के लिए थिएटर ने लोक नाटकों से प्रेरणा ली। और इसमें कुछ ग़लत भी नहीं था। इस मामले में हमारे गुरू हैं हबीब तनवीर। उन्होंने बहुत पहले आगरा बाज़ार जैसे नाटक किए। लोक संगीत पर आधारित। पर अब यह बात ख़त्म हो रही है तो अच्छी बात है। क्यों कि अब और भी आगे की चीज़ें आने लगी हैं। और अब स्थिति अच्छी है। एक निर्देशिका अपने अभिनेता के बारे में विश्लेषण करती है। पर सोचिए एक समय वह भी था कि हिंदी के अवार्ड के लिए कोई अभिनेता नहीं मिलता था। बात फिर मुड़ी है और कारंत कह रहे हैं कि अब हिंदी रंगमंच पर बात भी हो रही है और जो कोई कहता है कि मैं संघर्ष कर रहा हूं तो यह सहज गुण है उसका। फ़िल्म में तो जो कोई संघर्ष कर रहा है वह अपने अकेले के लिए कर रहा है। पर रंगमंच में एक कोई अकेला संघर्ष नहीं करता।
थिएटर को आखिर संभव फिर से कैसे बनाया जाए? सवाल पर कारंत का कहना था कि अभी मुंबई में गांधी वर्सेज गांधी नाटक चल रहा है। पॉपुलर है। लेकिन हमारी राय में नाटक पॉपुलर होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है गर्मी पैदा करना। मैंने कर्नाटक में देखा अगर नाटक में सफल होना है तो पहले दर्शक चाहिए। तो दर्शकों को ध्यान में रख कर मैंने अभिनेता तैयार किए। पर दस साल बाद प्रसन्ना ने कहा कि दर्शकों के लिए नाटक देना चाहिए। यह आइडियालॉजी रखा। पर आज भी आइडियालॉजी को उतना महत्व मैं नहीं देता जितनी कि रंगमंच की गतिविधियों को। अब आप ही बताइए कि उत्तर प्रदेश में कई चीज़ें अस्थिर हैं। राजनीति में भी साहित्य में भी और कला में भी अस्थिरता होगी? आप बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है? तो सिर्फ़ एक थिएटर से ही एक अच्छी उम्मीद आप क्यों लगा बैठते हैं? मैं दिल्ली से निकल कर अपने गांव नहीं गया। एन.एस.डी. से बाहर मुझे सबसे पहला मौक़ा लखनऊ में ही मिला। हयवदन किया 1972 कि 73 में। सारे लखनऊ के लोगों को ले कर। मैं मानता हूं कि टी.वी. का भी यह शुरू-शुरू का असर है। जैसे हिंदी फ़िल्मों ने पारसी थिएटर को ख़त्म किया। राधेश्याम कथा वाचक का ज़ोर था तब। आगा हश्र कश्मीरी के नाटक चलते थे। पर हिंदी सिनेमा उनको खा गया। पारसी नाटक ख़त्म सा हो गया। पर नाटक नहीं। क्यों? क्यों कि पारसी थिएटर जो दिखाता था वही चीज़ फ़िल्म ज़्यादा अच्छी तरह से दिखाने लगी। तो पारसी थिएटर लोग क्यों देखते? ऐसे में हमने जयशंकर प्रसाद के नाटक करने शुरू किए। और आज भी हम पाते हैं कि प्रसाद के नाटक काफी महत्वपूर्ण हैं। खैर नाटकों में प्रगति तो हुई। पर तामझाम भी चला। पर तामझाम ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। यह बहुत पहले मोहन राकेश ने कहा था। दरअसल थिएटर में ह्यूमन वैल्यू ज़्यादा इम्पार्टेंट है। कोई न्यूज़ कहानी कैसे बनती है? एक राजा था, मर गया, यह न्यूज़ है। पर एक राजा मर गया, फिर उसके दुःख से रानी भी मर गई तो यह कहानी बन गई। पर अब हर कोई चाहता है कि नाटक को सशक्त बनाया जाए। तो नाटक का आलेख ही नहीं, मंच सज्जा, वेशभूषा, विज्ञापन, ब्रोसर में भी बहुत परिवर्तन करना पड़ेगा। अभी जो मंदी आ गई है थिएटर में उससे घबड़ाने की ज़रूरत नहीं है, वह स्वाभाविक है। पारसी थिएटर को जब फ़िल्मों ने खाया था, तो अंधकार सा छा गया था। साहित्यिक और मंचीय नाटक के विभेद ने भी मुश्किल में डाला था। मेरा कहना है कि अगर नाटक है तो साहित्यिक गुण होना चाहिए और साहित्यिक है तो नाटकीय गुण भी होना चाहिए।
कारंत कहते हैं कि एक समय खुद भी मैं भारतीय रंगमंच और हिंदी नाटक पर थीसिस लिखने वाला था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मेरे गाइड थे डॉ. जगन्नाथ प्रसाद शर्मा। पर मैंने थीसिस जमा नहीं की। पर तब मैंने भी कहा था कि प्रसाद का नाटक मंचीय नहीं है। पर एन.एस.डी. में जाने के बाद मुझे यह अपनी ही बात ग़लत लगी। और मैंने वहां प्रसाद के पांच-छह नाटक किए। तो प्रसाद के नाटकों को मंचीय न कहना मेरी ग़लती नहीं थी। दरअसल यह एक भ्रम था। और उसका कारण यह था कि प्रसाद के नाटक करने के लिए श्रम चाहिए, आसक्ति चाहिए। और यही लोगों में नहीं होता। इसी से लोग बचते हैं। तो कह देते हैं कि प्रसाद के नाटक मंचीय नहीं हैं। मैं अपनी बात कहूं तो इस समय मैं प्रसाद और भारतेंदु से बहुत प्रभावित हूं। प्रसाद और भारतेंदु मेरे लिए मूल धन हैं। और सबसे ज़्यादा इन्हीं के नाटक मैंने किए भी। क्यों कि इनका नाटक बड़ी डिमांड करता था, ट्रेनिंग की।
आप जो कहते हैं कि रंगमंच सुधारने की बात तो अगर मैं कहूं कि सब जगह रंगमंच सुधार दूंगा तो यह बहुत बड़ा अहंकार होगा ना ! दरअसल हिंदी रंगमंच को सुधारने के लिए दर्शक चाहिए। और दर्शक बनाने के लिए मैं सबसे पहले योग्य नाटक खोजूंगा। अभिनेता नहीं खोजूंगा। जो हैं उन्हीं से काम कराऊंगा। जैसे सबसे पहले मैंने लखनऊ में हयवदन किया तो पद्मिनी की भूमिका के लिए मैंने शोभना को चुना था। आज वह दूरदर्शन दिल्ली में समाचार वाचिका है। पर तब वह पढ़ रही थी बी. ए. में। अनिल रस्तोगी को लिया, कपिल बनाया था। विजय वास्तव को देवदत्त बनाया था। यह सभी नए थे। हल्लो भइया को लिया। नाटक में हल्लो-हल्लो आता है। तभी से उसका नाम हल्लो भइया पड़ गया। हयवदन नाटक कठिन था, शरीर किसी का, मस्तक किसी का इस बात को नए कलाकारों के मार्फ़त कहना आसान नहीं था। लेकिन मैंने किया। नए लोगों को ले कर किया। क्या आज भी अगर लखनऊ का रंगमंच सुधारने के लिए आप को बुलाया जाए तो क्या आप आना चाहेंगे? कारंत बोले, सरकार के कहने से नहीं। रंगमंच वाले बुलाएं तो आ जाऊंगा।
कारंत अपने रंगकर्म यात्रा के बाबत बताते हैं कि मैं हिंदी प्रचारक था। और ठीक से हिंदी सीखने के लिए बनारस आया था। संगीत भी वहीं सीखा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी में अपना नाम लिखाया। तब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वहां मेरे अध्यापक थे। नामवर भी थे। और जब नाटक पर थीसिस लिखने की बात आई तो मुझे लगा कि नाटक को भी समझ लेना चाहिए। तो नाटक को समझने के लिए मैं नेशनल स्कूल ऑफ़ ड्रामा दिल्ली गया। मैं तब 32 वर्ष का था। और प्रोफेसर बनना चाहता था। और भारतीय रंगमंच पर अपने शोध को पुख्ता बनाने के लिए नाटक की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। पर देखिए विधि ने कहां से कहां पहुंचा दिया। तीन साल एन.एस.डी. में पढ़ाई करने के बाद भी कर्नाटक वापस नहीं गया। दिल्ली में ही रहा। एक स्कूल में काम करने लगा। वहां भी नाटक ही सिखाता था। फिर तब का दिन है और आज का दिन कि मैंने फिर पीछे मुड़ कर नहीं देखा। और नाटक ने मुझे छोड़ा नहीं। आज मैं जब भी सोचता हूं थिएटर ही सोचता हूं, कुछ और नहीं। मैं संगीत भी जानता हूं। बाक़ायदा। पर कभी संगीत की बैठक करूं। यह कभी मन में नहीं आया। हालांकि थिएटर करता हूं तो कई बार मुझे लगता है कि मैं रिपीट कर रहा हूं। पर संगीत में मैं अपने को रिपीट करता नहीं पाता। बावजूद इसके मैं संगीत छोड़ सकता हूं। लेकिन थिएटर नहीं। अब यह बात भी ज़रूर है कि थिएटर बिना संगीत के नहीं होता ना ! जब कि संगीत बिना थिएटर के भी हो सकता है। तो मैं थिएटर ही हरदम करते रहना चाहता हूं। क्यों कि इसमें संगीत भी है और थिएटर भी। शायद इसी लिए इन दिनों मैं लाइट एंड साउंड प्रोग्राम भी करने लगा हूं। जिसमें थिएटर और संगीत दोनों की ही अनिवार्यता होती है।
(बातचीत राष्ट्रीय सहारा से साभार. 1998 में लिया गया इन्टरव्यू) FB
FB Twitter
Twitter