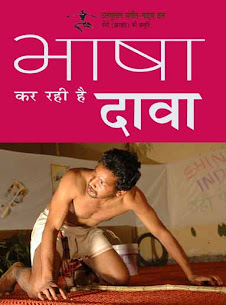कला के क्षेत्र में ‘ब्लैकफेस’ रंगमंच की खोज 1830 के आसपास अमेरिकन थिएटर ने की। मुख्यधारा में लोकप्रिय चरित्र टार्जन की खोज 1912 में एडगर राइस बर्रो ने की जो सिनेमा के पर्दे पर पहली बार 1918 में आई ‘टार्जन ऑफ द एप्स’ के रूप में। तब से लेकर आज तक टार्जन पर 200 से अधिक फिल्में बन चुकी हैं। टार्जन ने लोकप्रिय मनोरंजन उद्योग में जंगल और जंगल में रहने वालों को किसी बाहरी ग्रह के निवासियों की तरह परोसा जो दिखते तो इंसान की तरह हैं, मगर इंसान हैं नहीं। यह पूरा नजरिया ‘जंगल राज’ के रूप में सामने आता है। जंगल राज यानी एक ऐसी व्यवस्था जहां कोई व्यवस्था नहीं है। जहां लोग अराजक हैं, हिंसक हैं, बर्बर हैं, असभ्य हैं और जहां बलवान कमजोर को मारकर खा जाता है। वहीं, कला, साहित्य और सिनेमा में, यानी मनोरंजन और विज्ञापनों के बाजार में इस जंगल राज को या जंगलीपन को ‘वाइल्डनेस’ के रूप में बेचा जाता है। वाइल्डनेस का यहां अर्थ सिर्फ और सिर्फ चरम उत्तेजना है। चरम बर्बरता की हद तक उत्तेजना। टार्जन टाइप की फिल्में और कंडोम एवं विभिन्न किस्म के बॉडी स्प्रे के विज्ञापन इसके सबसे बढ़िया उदाहरण हैं।
भारतीय फिल्मों में जंगली यानी आदिवासियों पर केन्द्रित पहली फिल्म ‘इज्जत’ 1936 में बनी। इसे फ्रैंज ऑस्टन ने निर्देशित और हिमांशु राय ने प्रस्तुत किया था। उस समय की स्टार और बोल्ड अभिनेत्राी देविका रानी ने इसमें भील आदिवासी युवती और जानेमाने कलाकार अशोक कुमार ने भील युवक की भूमिका निभायी थी। फिल्म को प्रोड्यूस किया था बॉम्बे टॉकीज ने। टार्जन की पॉपुलर छवि वाली पहली फिल्म भी ‘इज्जत’ के साथ-साथ ही 1937 में आई। होमी वाडिया के निर्देशन में वाडिया मूवीटोन कंपनी ने ‘तूफानी टार्जन’ नाम से पहली टार्जन फिल्म बनायी। यह हिंदी के साथ-साथ तमिल में भी प्रदर्शित हुई थी। इसमें एक आदिवासी कैरेक्टर ‘दादा’ को जिसकी भूमिका बोमन श्राफ ने की है, जिसे फिल्म में आधा आदमी आधा वनमानुष बताया गया है। 1937 से 2000 तक भारतीय फिल्मोद्योग ने टार्जन कैरेक्टर वाली 22 फिल्मों का निर्माण किया है।
अब तक आदिवासी जीवन व समाज को किसी न किसी रूप में परंतु प्रमुखता से चित्रित करने वाले फिल्मों की संख्या 100 से ज्यादा हैं। इसमें उन फिल्मों की गिनती शामिल नहीं है, जिनमें आदिवासी चरित्रों को सिर्फ नाच-गान यानी ‘झींगा ला-ला हुर्र, हुर्र ...’ करते हुए दिखाया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय फिल्मोद्योग और पॉपुलर कल्चर का अरबों रुपये का बाजार नस्लीय रंगभेद, जातिगत पूर्वाग्रहों और धार्मिक एवं लैंगिक उत्पीड़न पर खड़ा है।
बहुजातीय संस्कृति वाले भारतीय समाज में एक धर्म, एक संस्कृति, एक भाषा का नस्लीय फिल्मी मनोरंजन का बाजार खड़ा करने का काम दादा फाल्के ने किया। सिनेमा और फाल्के के आने के पहले मनोरंजन का पॉपुलर बाजार पारसी थिएटर और नौटंकी कंपनियां थीं। जिनमें डाकुओं, ऐतिहासिक किस्से और ऐय्यारों का ड्रामा हुआ करता था। रामलीला और रासलीला जैसी नाट्य परंपराएं मनोरंजन के बाजार की बजाय विशुद्ध रूप से धार्मिक अवसरों से जुड़े थे। फाल्के ने 1917 में ‘लंका दहन’ बना कर धर्म को मनोरंजन के सिनेमाई बाजार में बदलने का काम किया। 1913 में आई ‘हरिश्चंद्र तारामति’ के बाद ‘लंका दहन’ उनकी दूसरी फिल्म थी जिसकी ब्लॉकबस्टर कमाई ने मनोरंजन के बाजार में धार्मिक यानी नस्लीय ट्रेंड को पूरी तरह से स्थापित कर दिया। और ‘लंका दहन’ के आठ साल बाद 1925 में 27 सितंबर को भारत के बहुसंख्यक नस्लवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। विजयादशमी के दिन। यानी रावण वध के दिन। अनार्य राक्षसों, असुरों, आदिवासियों के संहार के पारंपरिक वार्षिक उत्सव दशहरा के दिन।
20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका में एक ऐसी फिल्म आई जिसे फिल्मी इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग दुनिया का पहला फुल लेंथ फीचर फिल्म मानता हैै। डी. डब्ल्यू. ग्रिफिथ (1875-1948) की फिल्म ‘द बर्थ ऑफ ए नेशन’ (1915) निःसंदेह सिने ताकत और कला की बेजोड़ प्रस्तुति है। पर इसी के साथ यह दुनिया की सबसे नस्लीय फिल्म भी है। जिसमें गोरों का महिमामंडन और काले लोगों का स्टीरियोटाइप नकारात्मक चित्रण हुआ है। क्या यह महज संयोग है कि ठीक इसी समय भारत में दादा फाल्के ‘लंका दहन’ (1917) बनाते हैं जो नस्लीय और धार्मिक फिल्म है। जिसमें असुर आदिवासियों की हत्या करने वाले आर्यों का महिमांमंडन करते हुए ब्राह्मणवादी मूल्यों का गुणगान किया गया है। वास्तव में दादा फाल्के भारतीय सिनेमा के नहीं हिन्दू सिनेमा के ‘पिता’ हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ धार्मिक और मिथकीय फिल्में बनायी और सिनेमा कला के जरिए हिंदू धर्म का प्रचार-प्रसार किया। दादा फाल्के ने भारत की साझी सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत की अवहेलना ही नहीं की बल्कि अपनी फिल्मों से नस्लीय भेदभाव और हिंसा को भी भरपूर खाद-पानी दिया। उनकी सारी फिल्में देश के मूलनिवासियों, आदिवासियों, राक्षसों और असुरों की हत्याओं का महिमामंडन करती हैं।
1909 में पंजाब में सबसे पहले और फिर 1910 में अखिल भारतीय स्तर पर एक राजनीतिक पार्टी के रूप में हिंदू महासभा का गठन हुआ। हमें बताया जाता है कि 1909 में मुस्लिम लीग की स्थापना की प्रतिक्रिया में हिंदू महासभा अस्तित्व में आया। इसके बाद 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होती है और आदिवासी इलाके में हमें वनवासी कल्याण आश्रम पहली बार 1952 में दिखाई देता है। इसी समय यानी 1953 में ‘जंगल का जवाहर’ सिनेमाघरों में प्रदर्शित होती है जिसमें जंगली लोगों की सेवा करने वाले एक डॉक्टर और उसकी बेटी के एडवेंचरस कारनामों को होमी वाडिया ने ग्लैमरस तरीके से प्रस्तुत किया है। साथ ही 1954 में क्लासिक मानी जानेवाली ‘प्रगतिशील’ बिजन भट्टाचार्य की कहानी पर बनी हिंदी फिल्म ‘नागिन’ आती है जिसमें आदिवासियों को ‘जहर बेचनेवाला’ बताया जाता है। ध्यान रहे कि यह वही समय है जब दक्षिण के तेलंगाना, पूरब के तेभागा व (तत्कालीन मध्यप्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सहित) ग्रेटर झारखंड और उत्तर-पूर्व के आदिवासी अपने नैसर्गिक पुरखा अधिकारों व स्वायत्तता की लड़ाई लड़ रहे थे। उसी समय में वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना आरएसएस ने सरकार के सहयोग से तत्कालीन मध्यप्रदेश के जशपुर में की थी। जबकि विश्व हिंदू परिषद 29 अगस्त 1964 को अस्तित्व में आता है।
बीसवीं सदी के दूसरे दशक से लेकर सातवें दशक तक में हुए हिंदू नस्लवादी संगठन के सामाजिक और राजनीतिक उभार व गठन के पीछे फाल्के की नस्लीय फिल्मी परंपरा की भयावह भूमिका है। हिमांशु राय, होमी वाडिया, बिमल राय, सत्यजीत रे, बिजन भट्टाचार्य, ऋत्विक घटक, राजेन्द्र सिंह बेदी, ख्वाजा अहमद अब्बास और तमिल के आर नारायण मूर्ति जैसे गंभीर व प्रगतिशील माने जानेवाले फिल्मकार और लेखक नस्लीय परंपरा के इस यथास्थितिवाद को अपनी फिल्मों से बनाये रखते हैं।
इस दृष्टि से 2015 तक की 10 भारतीय नस्लवादी फिल्में निम्नांकित हैं जिनमें आदिवासियों का स्टीरियोटाइप नकारात्मक और नस्लीय चित्रण हुआ है -
1. नागिन (1954) हिंदी
2. अरण्येर दिनरात्रि (1970) बांग्ला
3. ये गुलिस्तां हमारा (1972) हिंदी
4. अल्लुरी सीताराम राजु (1974) तेलुगू
5. आक्रोश (1980) हिंदी
6. मैसी साहब (1985) हिंदी
7. टैंगो चार्ली (2005) हिंदी
8. ओंगा (2012) ओड़िया/हिंदी
9. अरवान (2012) मलयालम/तेलुगू
10. मैसेंजर ऑफ गॉड-2 (2015) हिंदी
1954 में रिलीज हुई बॉलीवुड की ‘नागिन’ संभवतः उत्तर-पूर्व की झलक दिखलाने वाली पहली पॉपुलर मसाला फिल्म है। बॉलीवुड निर्मित अन्य चार फिल्में हैं - ‘ये गुलिस्तां हमारा’ (1972), ‘दिल से’ (1998), ‘टैंगो चार्ली’ (2005) और ऑस्कर के लिए 2014 में भारत की ओर से भेजी गयी ‘लियर्स डाइस’ (2013)। ‘नागिन’ फिल्म की शुरुआत इन शब्दों के साथ होती है कि ‘यह फिल्म किसी भी मौजूदा या पुरानी जाति के जीवन से संबंध नहीं रखती’। लेकिन फिल्म का पहला ही दृश्य अपने कॉस्ट्यूम्स और प्रॉपर्टी के जरिए बता देता है कि यह उत्तर-पूर्व के आदिवासियों की कहानी है। फिल्म में दो कबीले बताए गए हैं जो जहर का व्यापार करते हैं और व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता के चलते दोनों एकदूसरे के खून के प्यासे हैं। सबसे सोचनीय पक्ष यह है कि फिल्म की कहानी प्रगतिशील वामपंथी नाटककार बिजन भट्टाचार्य ने लिखी है। गैर-आदिवासी समाज का दक्षिणपंथी हो या वामपंथी वह आदिवासियों के प्रति कैसी दृष्टि रखता है और उनसे किस हद तक नस्लीय घृणा करता है, इसका सिनेमाई दस्तावेज है ‘नागिन’।
इसी तरह 1972 में आई देवानंद अभिनीत और आत्माराम निर्देशित ‘ये गुलिस्तां हमारा’ भारत-चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर है। इसमें भी उत्तर-पूर्व के आदिवासियों को देश के लिए जहरीला यानी ‘देशद्रोही’ के रूप में दर्शाया गया है। इसका एक गाना ‘मेरा नाम आओ ...’ सीधे-सीधे अरुणाचल के ‘आओ’ आदिवासियों पर केन्द्रित थी जिसे उत्तर-पूर्व के आदिवासियों के विरोध के कारण संपादित करना पड़ा था। ‘टैंगो चार्ली’ (2005) में भी उत्तर-पूर्व के विद्रोही आदिवासियों को इसी तरह से दिखाया गया जिसे उत्तर-पूर्व में जबरदस्त विरोध के कारण प्रतिबंधित करना पड़ा।
2014 में भारत की ओर से ऑस्कर को भेजी गई फिल्म ‘लियर्स डाइस’ हिमाचल की पृष्ठभूमि पर है। इसमें एक पहाड़िन महिला अपनी बच्ची के साथ दिल्ली में मजदूरी करने आए और फिर गुम हो गए पति को ढूंढने आती है। उसकी इस तलाश में सेना का एक भगोड़ा सिपाही साथ देता है। मतलब फिल्म बताती है कि सेना ही उत्तर-पूर्व के आदिवासियों की रक्षक है। सेना का भगोड़ा फौजी भी कितना ‘मानवीय’ होता है ‘लियर्स डाइस’ दर्शकों को यही बताती है। यहां यह याद रखना होगा कि उत्तर-पूर्व के आदिवासी ‘आफ्सपा’ जैसा कानून और अपने इलाके से सेना को हटाने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं।
- अश्विनी कुमार पंकज
(यह लेख ‘फॉरवर्ड प्रेस’ के अप्रैल 2016 अंक में छपा है.)

 FB
FB Twitter
Twitter